अपनी एक व्यंग्य रचना - कोहरा और विकास की रेल- 'लफ्ज़' के ताज़ा अंक में आई है !
कोहरा और विकास की रेल
शीत लहर और कुहरे से ज़्यादा टिकट कन्फर्म न हो पाने की आशंका से कांपते मन और शरीर को उस वक़्त बड़ी गर्माहट का अहसास हुआ जब एक मित्र ने कहीं से एक कन्फर्म तत्काल टिकट जुगाड़ दिया. हवाई जहाज से कुछ ही कम कीमत अदा करने के बावजूद ये सौदा महंगा नहीं लगा क्योंकि ऑफिस से मिली छुट्टियां दो रोज़ पहले ही खर्च हो चुकी थीं. मोबाइल फोन पर रेल विभाग से ये जानकारी हासिल कर कि ट्रेन चार घंटे विलम्ब से छूटेगी, समय का हिसाब जोड़-घटाने के बाद अपना सामान और मन में इत्मीनान लिए मैं स्टेशन पहुँच गया.
प्लेटफार्म पर देश की आबादी के अनुपात में ही यात्री लोग मौजूद थे. बाहर ‘कमाने’ निकले देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्थात युवा शक्ति का प्रतिशत कुछ अधिक ही था जो सस्ती जींस जैकेट पर मफलर कसे, सूटकेस-थैलों में सत्तू-चिवडा और चेहरे पर बदहवासी लादे यहाँ-वहां टहल रहे थे. चादरें बिछी हुई थीं, जिनपर इंसान सामानों की तरह ही बिखरे पड़े थे. कभी कोई एक आदमी उचक कर प्लेटफार्म के किसी छोर पर गुम होती रेल लाइन की और देखने लगता तो बाकी सारी गर्दनें एक लय में उसी ओर लचक जातीं. घोषित विलम्ब के चार घंटों की मीयाद पूरी होने के बावजूद ट्रेन का कोई पता नहीं था. हालांकि स्टेशन पर लगे दर्जनों लाउडस्पीकर निरंतर गाड़ियों की आवाजाही, बल्कि देरी से आने की सूचना लगातार और बार-बार दे रहे रहे थे. पर उसमें हमारी गाड़ी की कोई चर्चा नहीं थी. उसी वक़्त प्लेटफार्म पर एक ऐसी गाड़ी आ खड़ी हुई जिसे वहां उपलब्ध सूचना के मुताबिक हमारी वाली गाड़ी से घंटे भर बाद प्रस्थान करना था. सामने बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो पल-पल बदलती स्थिति बयान कर रहा था, अब भी जिद पर अडा था कि हमारी गाडी भी इसी प्लेटफार्म से चंद मिनटों में ही छूटेगी. कुल मिला कर बेहद रहस्य- रोमांच से लबरेज स्थिति थी. अगले आधे घंटे तक इस स्क्रीन को एकटक देखने और लाउडस्पीकर की उद्घोषणा का शब्द-शब्द सुनने के बाद स्पष्ट हुआ कि हमारी ट्रेन को आखिरकार ढाई घंटे और देर से आने की छूट मिल गयी है. मैंने ठीक स्क्रीन के सामने धरने की मुद्रा में बैठ कर एक पत्रिका खोल ली और पढ़ने का उपक्रम करने लगा.
मुझसे तकरीबन चिपक कर बैठे सज्जन, जो वाकई सज्जन थे क्योंकि मेरे आग्रह पर उस प्राइम लोकेशन पर उन्होंने अपने लिए भी नाकाफी जगह का आधा हिस्सा मुझे दे दिया था, मेरी हरकतों
से समझ गए थे कि मुझे क्या तक़लीफ है। गम का फ़साना तेरा भी है, मेरा भी- वाली आत्मियता के साथ उन्होंने अपने साथ कुछ बिस्किट का साझा करने का आमंत्रण दिया जिसे मैंने अभी-अभी रेलवे की उद्घोषणा में सुनी एक चेतावनी के मद्देनज़र ठुकरा दिया। इसका बुरा न मानते हुए वे एक लम्बी साँस लेकर बोले, "काश। हम अपनी गाडी से निकल गए होते..अब तो लगता है बरात बिदा होने बाद ही पहुंचेंगे।"
से समझ गए थे कि मुझे क्या तक़लीफ है। गम का फ़साना तेरा भी है, मेरा भी- वाली आत्मियता के साथ उन्होंने अपने साथ कुछ बिस्किट का साझा करने का आमंत्रण दिया जिसे मैंने अभी-अभी रेलवे की उद्घोषणा में सुनी एक चेतावनी के मद्देनज़र ठुकरा दिया। इसका बुरा न मानते हुए वे एक लम्बी साँस लेकर बोले, "काश। हम अपनी गाडी से निकल गए होते..अब तो लगता है बरात बिदा होने बाद ही पहुंचेंगे।"
फिर बातचीत के क्रम में मालूम हुआ कि वे चचेरे भाई की शादी में अपने गाँव जा रहे थे. बीस घंटे की यात्रा के बाद दोपहर बरात निकलने तक पहुँचने के लिए मेरी तरह ही उन्होंने “तत्काल-मार्ग” अपनाया था. पर अब तो! खैर! और दूसरी जो बात स्पष्ट हुई वो ये थी कि जिस अपनी गाड़ी से निकलने के इरादे का ज़िक्र वो कर रहे थे वो दो पहिये पर चलती है. उन्होंने बताया कि रेलों की ऐसी हरकतों के कारण ही वे कई बार अपने दुपहिये पर अपने गाँव तक का रास्ता तय कर चुके हैं. मोटर साइकिल पर इस सर्दी में डेढ़ हज़ार मील शादी में शिरक़त करने जाने का हौसला रखने वाले इस वीर पुरुष को देखते हुए एकबारगी मुझे अपने देश में रिश्तों की जबरदस्त चुम्बकीय शक्ति पर आश्चर्य-मिश्रित गर्व हुआ.
अपने देश में वक़्त काटना कभी कोई समस्या नहीं रही. रेलवे प्लेटफार्म तो ख़ास इसी काम के लिए बनाए जाते हैं. वक़्त की फसल खूब होती है हमारे यहाँ, जिसे लोग दफ्तर, चाय की दूकान, पार्क या फुटपाथ की बेंच या घर पर यूं ही बैठे-बैठे काटते रहते हैं. मैं जहां था वहां तो फिर भी एक ठीक-ठाक जलसे सा माहौल था। दूसरे को काम करते देखते हुए खुद बेकार वक़्त काटने में थोड़ी नैतिक पीड़ा हो सकती है. पर यहाँ वो समस्या भी नहीं थी क्योंकि हर शख्स ठलुआ बैठा था. ढाई-तीन घंटे तो यूं ही चुटकियों में दस-बीस करवटें बदलते काटे जा सकते थे। फिर आस-पास रेहड़ियों पर बाकायदा पैकेटों में ‘टाइम-पास’ नामक कई वस्तुएं बिक रही थीं। आलू की चिप्स और मूंगफलियों की शक्ल की कुछ ऎसी चीजें लेकर मैं भी टूंगने लगा. इस छोटे से उद्योग से सचमुच मेरे दस मिनट मजे में कट गए.
आप किसी ऐसी जगह बैठे हों जहां बहुत से लोग कुछ नहीं, बस इंतज़ार कर रहे हों तो थोड़े-थोड़े अंतराल पर ऊब के दौरे पड़ना भी स्वाभाविक है. आदमी अपनी इस प्रकृति के वाकिफ है सो उसने मोबाइल ईजाद कर लिया है. इस चीज़ को हथेली में लेकर आप ऊबते हुये भी व्यस्त रहने का भ्रम पाल सकते हैं। अपने ईर्द-गिर्द एक भरी-पूरी दुनिया की मौजूदगी के अहसास को नकारते हुए इसकी स्क्रीन पर नज़र गडाए लगभग तीस फीसदी सहयात्री इसी जद्दोजहद में थे, पर बीच बीच में अपनी स्क्रीन से निगाह उठा कर रेलवे वाली स्क्रीन पर फेर देना उनको वातावरण से जोड़े हुए थे. मैंने मन ही मन अनुमान लगाना चाहा कि इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के विभिन्न स्टेशनों पर देर से चलती गाड़ियों के यात्री कितना वक़्त काट चुके होंगे और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पडा होगा. इस सवाल पर मुझे अर्थशास्त्र के तमाम सिद्धांत भी इसी बिखरी हुई भीड़ में कहीं ऊंघते नज़र आये.
ट्रेन भी आखिर जाती कहाँ? अधिक से अधिक प्लेटफार्म बदल सकती थी, सो चार घंटे बीतने के बाद अपने पुनर्निर्धारित समय से दस मिनट पहले प्लेटफार्म नं एक पर आने के अपने वादे से मुकर गयी और पांच नंबर पर आने को मचली. इस उद्देश्य की उद्घोषणा होते ही मैं भी अन्य सवारियों के साथ सामान अपने शरीर के दीगर हिस्सों पर और पाँव सर पर रख कर पुल की और भागा. हलफ उठा कर कहता हूँ कि उस क्षण सिवा बज़रिये प्लेटफार्म नंबर पांच आने वाली ट्रेन में कहीं छुपे अपने बर्थ को हासिल कर लेने के सिवा मेरे मन में कोई विकार नहीं था. लक्ष्य-प्राप्ति के प्रति ऐसे समर्पण भाव मैंने अपने साथ दौड़ते हरेक नर नारी के अंग प्रत्यंग में देखा।
प्लेटफार्म पर पहुँच कर कुछ लम्बी साँसे लेने के बाद पाया कि बस इंतज़ार का लोकेशन बदल गया है, हमसफ़र वही हैं, बस इतने फर्क के साथ कि अब वो लेटे और ऊंघते हुए नहीं बल्कि खड़े और मुस्तैद हैं. यहाँ मेरी सोच ने ज़रा विस्तार लिया और देखा कि इस पूरे परिदृश्य को ज्यों का त्यों रखते हुए आने वाली ट्रेन को विकास और प्लेटफार्म को लक्ष्य कहा जाय तो आज़ादी के बाद के छः दशकों से लगातार यही रोमांचकारी खेल तो चलता आ रहा है. उधर प्लेटफार्मों पर भीड़ बढ़ती जा रही है. लोग विकास की रेल पर लटक कर भी जाने को आमादा हैं. ट्रेन कुछ मालूम और बहुत से नामालूम वजहों से लेट हुई जा रही है. एक ही पटरी पर किसिम-किसिम के उद्देश्य लादे ढेरों गाड़ियां आगे-पीछे और अक्सर एक दूसरे का रास्ता काटती चल रही हैं. सरकार कभी इसे रोककर उसे आगे बढ़ा देती है कभी उसे खड़ी कर उसे जाने देती है. इस ट्रेन को पांच सालों में उस स्टेशन तक पहुंचना है तो उसे दस सालों में उस लक्ष्य तक। अब नहीं पहुँच पा रहीं तो घोषणा कर समय आगे बढ़ाना पड़ता है। अक्सर घोषणा नहीं भी करते. कितना करें, जब रोज़ का यही हाल हो. अब तो पटरियां बदलने में भी मुश्किलें आ रहीं हैं कि वो खाली ही नहीं मिलतीं. इधर कुछ सालों से भ्रष्टाचार का कोहरा और घना हो गया है. हाई कमान के सिग्नल सिस्टम में भी लम्बी गड़बड़ी रही. बीच के किसी भी स्टेशन पर रोककर सुप्रीम कोर्ट या सी ए जी की चैकिंग शुरू हो जाती है। प्रजातंत्र में सिग्नल सिस्टम की खरीद आम चुनाव के ज़रिये होती है। उसमें भी घपला हो जाय तो क्या कीजे। ज्यादातर लाल ही रहने वाली बत्तियां खरीद ली जाती हैं. गाडी चले भी तो रफ़्तार नहीं पकड़ पाती। उधर बेताब जनता जहाँ-तहां जंजीर खींच कर रेल रोकती और उसपर लदती जा रही है।
कहाँ तक गिनाएं कि देश के विकास की गाडी किस-किस वज्ह से लुढ़कती चाल से चलने को मज़बूर है. अब तो जानकारों से भी पूछने की जरुरत नहीं, सब जानते हैं कि कुछ विशेष लक्ष्यों की ओर कुछ ख़ास लोगों को लेकर दौड़ने वाली राजधानी- शताब्दी कहलाने वाली गाड़ियां आम जनता की विकास रेलों को आउटर सिग्नल पर रुकवा कर आगे निकाल दी जाती है।
मैं सोच रहा हूँ कि उस वक़्त इसके सिवा कुछ कर नहीं सकता। आखिरी विकल्प यही है कि जाने का इरादा मुल्तवी कर घर लौट जाऊं। पर जानता हूँ ये विकल्प मेरे लिए नहीं है। तत्काल टिकट को कैंसल कराओ तो रिफंड भी नहीं मिलता। जीवन में इस तरह कितनी ही यात्राएं स्थगित या परिवर्तित करनी पड़ी हैं। विकास करने या आगे बढ़ने के सिवा कोई और विकल्प होता भी है क्या?
इतनी देर सोचते हो गए पर ट्रेन अब भी नहीं आई। हो सकता है आये ही न। ये भी सम्भव है कि कुछ ही देर में उद्घोषणा हो कि ट्रेन बजाय पांच नंबर अब तेरह नंबर पर आएगी। हम फिर झुण्ड बनाकर दौड़ पड़ेंगे। मेरा सहयात्री एकबारगी अपनी निजी मोटरसाइकिल पर अपना लक्ष्य साधने का मंसूबा बांधेगा और हताश होकर खोल देगा. प्लेटफार्म पर पहले से भी ज़ियादा भीड़ होगी। अचानक कोहरा बढ़कर प्लेटफार्म को भी ढक लेगा।
मेरी इस संभ्रम की-सी स्थिति के बीच ही उम्मीद की एक किरण-सी ट्रेन प्लेटफार्म में दाखिल होने लगी।

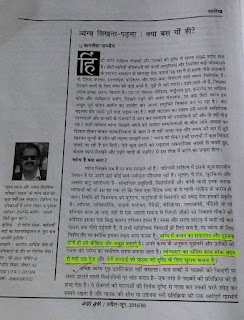

Comments