एक था गधा उर्फ़ शरद जोशी के नाटक में हम
शरद जोशी का मशहूर नाटक "एक था गधा उर्फ अलादाद खान" की अपनी मंडली के साथ मंच पर प्रस्तुति के बाद एक व्यंग्यात्मक आलेख लिखना बनता था. कुछ देर से सही, लिख पाया . .....
नाटक हमारे लिए कोई अजूबा नहीं था. बाबू-जीवन के हर चरण में कोई न कोई
नाटक चलता ही रहता है. अलग से एक नाटक खेलने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये एक सवाल है
जिसका जवाब अभी ढूँढा जा रहा है. थियेटर किस चिड़िया का नाम है ये हम जानते थे
क्योंकि देख रखा था. हमेशा बर्ड-वाचिंग के अंदाज़ में मंडी हाउस के थियेटरों की ओर
जाते और अन्य कई चीजों के अलावा नाटक भी देख लेते थे. इतना पक्के तौर पर मालूम था
कि इसमें एक मंच होता है जिस पर कुछ लोग नाटकीय अंदाज़ में चलते-बोलते रहते हैं.
रटे-रटाए सम्वाद और उसपर से ‘जो भूले सो याद कराया’ की सुविधा के साथ विंग्स में छुपा प्रोम्प्टर. ये कौन-सा
मुश्किल काम था जब हम जब चाहे बिना स्क्रिप्ट ही बॉस और बीबी दोनों को अपने सहज
अभिनय से झूठ सच की सीमा पर भटकाते रहते हैं.
वैसे ये नाटक “एक था गधा उर्फ अलादाद खान” सोच समझ कर नहीं चुना गया था पर आख़िरकार सटीक साबित हुआ. ये
अच्छा रहा कि नाटक के शीर्षक के आधार पर जो केन्द्रीय पात्र होना चाहिए था वह नाटक
में सशरीर उपस्थित नहीं था वरना इसकी भूमिका करने के लिए उपयुक्तता के आधार पर हम
सब खरे उतरते थे, यानी एक को चुनना चुनौती होता. पत्थरो को तराशने का हुनर और
धैर्य से युक्त एक प्रतिभावान निर्देशक भी हम चार-पांच सम्भावित नाट्य कर्मियों से
आ जुड़े थे. हिम्मत और उत्साह तो पहले से ही सबमें काफी मात्रा में था. बाक़ी काम
यानी नाटक लिखना शरद जोशी पहले ही कर चुके थे. ये समझने के लिए कि शरद जोशी ने ऐसा
क्यों किया, हमलोग नाटक को पढने में जुट गए. इस कोशिश में कई नई बातें मालूम हुईं
मसलन अन्य नाटकों की तरह इसमें भी संवाद हैं और एक अदद रामकली सहित ढेरों पात्र
हैं. इस नाटक का गधा इसकी आत्मा था. एक नवाब, कोतवाल, दरबारी और चिंतकों समेत
सत्ता का पूरा तामझाम था तो दूसरी ओर धोबी, दर्जी, पानवाले के साथ नागरिकों का भी
इंतज़ाम था. कहानी इतनी सी थी कि कोतवाल की गफलत से अलादाद नामक गधे की मौत नवाब
साहब के दरबार में अलादाद नामक आदमी की मौत की अफवाह फैला देती है. नवाब इस आदमी
के जनाजे को खुद कंधा देने का ऐलान करने के बाद जान पाते हैं कि अलादाद तो एक गधा
था. तब एक अलादाद नामक आदमी को पकड़ कर फांसी दी जाती है ताकि सत्ता की जुबान खाली
न जाए. ये राहत की बात थी कि नाटक का मर्म सबकी समझ में आ गया था पर हिन्दी
संवादों को पढने में सबको होती सामान्य पीड़ा को देख शुरू में हमारी हिम्मत ज़रा
डगमगाई ज़रूर वरना शुरू में तो हमारे उफनते उत्साह को यकीन था कि हम चार पांच लोगों
की टीम ही मिलकर पूरा नाटक कर गुजरेगी.
यहाँ से सम्भावित पात्रों की धर-पकड़ शुरू हो गई. नाटक मंडली रिहर्सल करने
के इरादे से कॉलोनी के चौपाल-नुमा स्थान पर छुट्टियों के दिन ज़मने लगी. यहां वह हर
आते जाते को बहला-फुसला कर एक भूमिका हथिया लेने के लिए उकसाती. उत्साही मंडली में
कुछ ने अपने मित्रों और पड़ोसियों को समझा-बुझा या धमका कर रिहर्सल में शामिल कर
लिया. उन्हीं में से एक यानी मुझे अपने कार-पूल के चार सदस्यों में नाटक के चार
पात्रों की छवि दिखने लगी. इन मित्रों ने भी महसूस किया कि रोज कार में मुझसे नाटक
का बखान सुनने से तो यही बेहतर होगा कि नाटक ही कर लिया जाय. आगे चलकर तो हालात
इतने उज्जवल हुए कि चार पात्रों की रिहर्सल चलती कार में होने लगी और एक रोज जब
दिल्ली जोरदार बारिश में स्वीमिंग पूल बनी हुई थी, हमारी कार-पूल ढाई घंटे जाम
में फँसी रिहर्सल में मशगूल रही.
लोग आते गए, कारवां बनता गया. चार से आठ,
आठ से दस...फिर
बस. रामकली ढूंढें न मिली. ये मोहतरमा नाटक के कोतवाल की प्रेमिका होती थीं. नाटक
में इनका न होना तय होने से कोतवाल की भूमिका के लिए होने वाली संभावित सर-फुटौवल
टल गई और ये भूमिका महज डील-डौल के आधार पर खाकसार को मिल गई. बाकी पात्रों के
चुनाव में भी दिक्कत पेश नहीं आई क्योंकि हम सब की शक्लें किसी न किसी पात्र से
मिलती थी. अभिनय क्षमता को आधार बनाने का यों भी कोई मामला नहीं बनता था. हम सबको
अपनी अपनी शक्लों के बारे में इतनी गलतफहमी ज़रूर थी कि हर एक को दूसरे की भूमिका
अपने लिए ज़्यादा उपयुक्त मालूम होती थी.
अब जो जोर-शोर से रिहर्सल शुरू हुए तो सबने देखा कि ये तो बड़े मज़े की चीज़
है. दफ्तर से लौट कर घरेलू काम निबटाने का जो वक्त था, रिहर्सल उसी में होती थी. हममें से कुछ तो दफ्तर से सीधे
वहीँ आने लगे ताकि आदेशों और फरमाईशों से पूरी आज़ादी का लुत्फ़ लिया जा सके. दो एक
जो इतने साहसी नहीं थे, थोड़ी देर से रिहर्सल पर पंहुचते थे पर आगे नाटक में
यों रम जाते थे कि घर लौटने पर किसी के जागते रहने की कोई आशंका न रह जाए. राहत के
इस अहसास से नाटक मंडली थकी होने के बावजूद ऊर्जा से भरी रहती थी. उधर बीबियों ने
भी कोई खास आपत्ति नहीं की क्योंकि ये वक़्त उनके सीरियलों का होता था और उन्हें
बंद कराके समाचारों की बोरियत फैलाने वाले लोग ही इस नाट्य-कर्म में शामिल थे.
इस नाटक में एक ख़ासा बड़ा, कुछ थोड़े बड़े और ढेर सारे छोटे-छोटे पात्र थे. हममें
जो उम्र में सबसे बड़े थे उन्हें सबसे बड़ी वाली भूमिका स्वतः ही मिल गई,
जिसके नतीजे
में उनकी नींद हराम हो गई. ये साहब राह-चलते भी अपने संवाद रटते नज़र आने लगे. छोटी
भूमिकाएं करने वाले या तो रिहर्सल में आते नहीं थे, या आ जाते तो बड़े पात्रों को
संवाद याद कराते थे. कुछ हफ़्तों में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली गयी कि पात्रों ने
स्क्रिप्ट हाथ में लेकर सम्वाद बोलना छोड़ दिया, केवल प्रोम्प्टर की आवाज़ को
हर्फ़-ब-हर्फ़
दोहराने लगे.
जल्द ही छोटे पात्रों को बड़े पात्रों के सारे संवाद याद हो गए और रिहर्सलों में
उनके सम्वाद वही बोलने लगे. इस स्थिति का एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि नाटक में
निर्देशक महोदय की ज़रूरत नहीं रही. हर पात्र दूसरे को संवाद आदायगी के गुर सिखाता
नाटक के विकास में सहयोग करने लगा. विशेष दुर्गति मुख्य पात्र नवाब साहब की हुई जो
सुझावों की मार से अधमरे होकर नवाबी अंदाज़ ही भूल गए. एक बार एक उत्तेजना भरे
संवाद में उन्होंने अलादाद खान नामक आदमी की लाश की बजाय मूल गधे की ही मांग कर दी,
जिससे पहले तो
हम सकते में आ गए, पर मामला समझ में आने पर हंस हंस कर रिहर्सल की छुट्टी
कर दी. निर्देशन और सुझाव के मामले में तीन चिंतकों की भूमिका करने वाले पात्र
सबसे आगे रहे क्योंकि उनका काम इक्कठे ही चिंतन करना था और अपने हिस्से के चिंतन
से निबट कर वे इक्कठे ही निर्देशन के काम में जुट जाते. हम सब के सामूहिक निर्देशन
से नाटक वहीं पहुँच गया जहां से शुरू हुआ था.
पात्रों की
संख्या और गुणवत्ता को लेकर असली निर्देशक को बड़ी चिंताएं थी. नाटक का एक महत्त्वपूर्ण
पात्र लखनवी उर्दू बोलने वाला नत्थू दर्जी था, जिसकी भूमिका इस नाटक -मंचन के असली
सूत्रधार निमाई दा कर रहे थे. हमारे ख़याल से, जो कि निर्देशक के ख़याल से एकदम जुदा
था, दादा का गोलाई-युक्त उच्चारण संवादों
में जान डाल देता था. उनकी संवाद-अदायगी पर निर्देशक की आपत्तियों को हमने इस तर्क
से खारिज किया कि क्या दर्जी बंगाली नहीं होते? खैर, निर्देशक
को तो हर पात्र की संवाद अदायगी पर बराबर ही आपत्ति थी. अपने गधे की याद में
रोता-चिल्लाता जुग्गन धोबी उन्हें दिल से रोता नहीं मालूम होता था. उसे पंचम तक पंहुचाने
की कोशिश में वे खुद भी खूब गला फाड़ते रहे पर आखिर इस ख़याल पर सब्र कर लिया कि अगर
कहीं कोई जुग्गन होता तो कम से कम दिखता हू-ब-हू ऐसा ही. नाटक में नागरिक और दरबारी
जैसे कुछ पात्र जोड़े में थे जिनकी भूमिका करने को शुरू में कोई राजी नहीं था. आखिर
कुछ पार्ट टाइम उत्साही मिल ही गए. तब जोड़ों को इकहरा कर दिया गया और इन पात्रों
के संवाद दुगुने होकर कलाकारों की हौसला आफजाई करने लगे. उधर नाटक का एक पात्र ‘सूत्रधार’ भावों में डूब कर इतनी शिद्दत से अपने डायलाग बोलता कि उसके
संवाद महज़ दर्शकों को संबोधन हैं. हम सभी पात्र एक वक़्त में हाव भाव दर्शाने या
संवाद बोलने में से एक ही काम कर पाते थे. नवाब साहब ने एक अंदाज़ जिसमें एक हाथ
ऊपर और गर्दन एक ओर मुडी होती थी और एक लय में, जिसमें गुर्राहट सी आती थी, पूरी
महारत हासिल कर ली थी. वैसे हम सब मुर्गे की तरह गर्दन एक ओर उठा कर ही संवाद बोल
पाते थे, क्योंकि इसी मुद्रा में प्रोम्प्टर की आवाज़ सुनाई देती थी.
नाटक का
दिन करीब था. हमारी तैयारी देखकर निर्देशक ने शरद जोशी से क्षमा मांगी और एकदम सेंसर
की भूमिका में उतर गए. कटाई-छंटाई शुरू हुई तो पात्र और संवाद, प्रसंग-दर-प्रसंग
कट-कट कर गिरने लगे. कोतवाल यानी मैं जो रामकली के प्रसंगों के कट जाने से पहले ही
सदमे में था, अपने बचे-खुचे संवादों की रक्षा में लग गया. नाटक के इस मोड पर हम
सबको इकठ्ठे काफी मात्रा में शर्म आई और हम अपनी बाबू योनि की मूल प्रवृत्ति के
अनुरूप आखिरी दिन काम समेटने की कोशिश में लग गए.
अब जो हम लोग जागे तो कई रातें जागे और अपने-अपने संवाद अदायगी समेत रट लिए.
उत्साह का ये आलम था कि हर सीन में अगले सीन के संवाद भी याद आ जाते और बोल भी दिए
जाते. कई बार रिहर्सल में अगला सीन पिछले से पहले कर दिया गया. पर कहावत है न कि ‘करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान’. आखिरी दिनों में
नाटक का अक्श साफ-साफ उभरने लगा था. हाव-भाव और संवाद दोहराते-रटते आखिर हम तमाम जड़मति सुजानों में तब्दील हो ही गए.
कटा हुआ
नाटक भी अच्छी खासी चुनौती था. पर भागने का रास्ता पूरी तरह बंद था. नाटक कॉलोनी में
अपने परिवारों के सामने ही खेला जाना था सो नाटक खेलने और न खेलने दोनों हालातों
में हमारी नाकें तलवार पर टिकी थी. इसलिए हमने ‘मरता क्या न करता
की बजाय ‘करो या मरो’ वाली मुद्रा अपना
ली. जिस दिन नाटक हुआ, हम बस मंच पर टूट पड़े. निर्देशक ने जिहाद का नारा बुलंद
किया और हम खुल कर खेले. अभ्यास अपनी जगह, हम सब पूरी लय में जो जी चाहा करते गए.
सारी टूटी कड़ियाँ जुड गईं, सारे छूटे सूत्र मिल गए. भूले हुए संवादों के खाली
स्थानों पर अपने आप कुछ लफ़्ज़ों ने कब्ज़ा कर लिया. कई नए संवादों का सृजन हो गया और
नाटक को नए अर्थ और आयाम मिले. सामने बैठी भीड़ के लिए हिन्दी नाटक एक नई चीज़ थी और
उसने वैसे ही ग्रहण भी किया. कुछ लोग इसे ‘कामेडी सर्कस का
जादू’ समझ कर जगह-बे जगह हंस-हंस के समां बाँध गए. जो इस बात पर
हैरान थे कि हमलोग ये नाटक आखिर क्यों कर रहे हैं, उसी हैरानी की हालत में पूरा
नाटक देख गए. कुछ शाश्वत आलोचक किस्म के जीव नाटक की कमियां ढूँढने की कोशिश में
आखिर तक टिके और कमियों के विशाल ढेर के सामने घुटने टेक गए. हमारा नाटक दर्शक
दीर्घा पर एक रेले की तरह गुजर गया.
बाद में और
लोगों से पता चला कि नाटक बहुत बढ़िया बन पड़ा था.

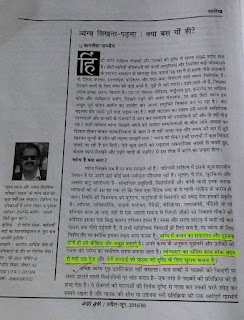

Comments