दाल और घर की मुर्गी
आज मुर्गी और दाल के बदले समीकरण पर थोडा चिंतन किया. “घर की मुर्गी दाल बराबर” वाले मुहावरे के जन्म-काल के समय इन दोनों वस्तुओं को बराबर कर देने वाला कौन सा तराज़ू इस्तेमाल किया गया था इस पर हिंदी भाषा का अर्थशास्त्र कुछ नहीं कहता। मुर्गी ही क्यों तोली गई, उसके शौहर मुर्गे को शोरबे में तब्दील करने का चलन तब तक नहीं था क्या? इन दोनों के मिले-जुले प्रयासों से बनने वाले गोल-गोल अंडे इस तुलनात्मक अध्ययन के दायरे में क्यों नहीं आये- ऐसे ही कुछ गंभीर और मौलिक सवाल मेरे जेहन में उभरे। ये तो तय है कि मुर्गी तब घर पर ही रहती थी और दाल के दाने भी रसोई के डिब्बे में ही पाए जाते थे. मुर्गी ज़रूर मौक़ा पाकर इन दाल के दानों को चुगती होगी, जिससे उसमें दाल का स्वाद आ जाता होगा. मुहावरेे में कहीं इसी वजह से उसे दाल बराबर न बता दिया गया हो।
तब से हालात में काफी अन्तर आया है. न मुर्गी घर पर रहती है न ही दाल रसोई के डिब्बे में. पहली बाज़ार से छील-तराश के तैयार आती है तो दूसरी अक्सर बाज़ार में छुपी बैठी होती है और ऊंची कीमत देने पर ही घूँघट हटाती है. उधर मुर्गी को भी गायब हो जाने का रोग है. ये रोग छठे-छमासे उसे बर्ड फ़्लू जैसी कुछ आयातित बीमारियों की छूत से लग जाता है. पर दाल से उलट तब मुर्गी सस्ती हो जाती है, भले ही उसे ग़रीब भी नहीं पूछते.
तब से हालात में काफी अन्तर आया है. न मुर्गी घर पर रहती है न ही दाल रसोई के डिब्बे में. पहली बाज़ार से छील-तराश के तैयार आती है तो दूसरी अक्सर बाज़ार में छुपी बैठी होती है और ऊंची कीमत देने पर ही घूँघट हटाती है. उधर मुर्गी को भी गायब हो जाने का रोग है. ये रोग छठे-छमासे उसे बर्ड फ़्लू जैसी कुछ आयातित बीमारियों की छूत से लग जाता है. पर दाल से उलट तब मुर्गी सस्ती हो जाती है, भले ही उसे ग़रीब भी नहीं पूछते.
दाल का हाल भी कुछ ठीक नहीं. अपने सबसे लोकप्रिय अरहरावतार में रोटी के संग मिलकर ये गरीबों का पेट भरने के काम आती रही है. ज्ञानी दाल में ही रोटी डुबाकर खाने के उपरांत प्रभु के गुण गाने की शिक्षा देते आये हैं. प्रभु-भक्तों की एक अलग जमात ने दालों को गोदामों में छुपा कर कीमते इतनी बढ़ा दीं कि सबके लिए प्रभु-गुण गाना दूभर हो गया. प्रभु-गुण गाने पर एकाधिकार रखने वाले भक्तों पर ही अब प्रभु कृपा करते हैं। यहाँ मुर्गी घर की हो या बाहर की कोई मदद नहीं कर सकती। प्रभु के मामले में मुर्गी का क्या काम?
दाल खिचडी बनाने में भी अनिवार्य मानी जाती है. मुझे संदेह है कि बीरबल की खिचड़ी पकने में इतनी देर इस लिए हुई कि वे पतीला चढ़ा कर दाल खरीदने बाज़ार गए होंगे. दाल मिली नहीं होगी, थक कर बादशाह के रसोईये से उधार लानी पड़ी होगी। उसने ये विकल्प ज़रूर दिया होगा कि खिचड़ी क्या खाना, दाल की बजाय मुर्गी ले जाएँ और बिरियानी बना लें। तमाम बुद्धिजीवियों की तरह ही उन्होंने सच को दर्शन से ढँकते हुए आरोप आंच और हांडी के फासले पर मढ़ दिया होगा।
दाल मिल भी जाए तो कई बार गलती नहीं। प्रेशर कुकर प्रेशर बनाये रखते हैं तो भी नहीं। राजनीति में तो अक्सर नमक ही नमकहरामी कर जाता है। दाल के और भी संकट हैं। दाल दाल में भी फ़र्क़ है। मखनी और फ्राई अवतारों के बरख्श ग़रीब की हांडी में छौंक को तरसती पतली दाल। बाज़ार इधर दाल से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है जैसे- उसके चिर संगी प्याज को भी छुपा कर। उधर मुर्गी बिन-प्याज़ा भी तंदूर में सिंक कर मज़ा दे जाती है। दाल और मुर्गी दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। ये ग़रीबों के लिए ज़रूरी होता है तो अघाये लोगों के लिए घातक। पर दाल से परहेज़ करने की सलाह दोनों किस्म के प्राणियों को दे दी जाती है।
दाल में काला ढूँढने वाले दाल और अर्थव्यवस्था को एकाकार देख पा रहे हैं। काले कारनामों के धब्बों से भरा अर्थतंत्र बरगलाते आंकड़ों और दावों के झक्क सफ़ेद जामे ओढ़ कर बैठा है। हक़ीक़त में इस अधगली पूरी काली दाल को लफ़्फ़ाज़ी की पीली परत से ढंकने की कोशिशें जारी हैं।
इस परिदृश्य में बिचारी घर की मुर्गी घूरे पर संकट में पड़ी दाल से अपने बिगड़े समीकरण पर चोंच बाए खड़ी है। ले दे कर एक ही प्रचलित मुहावरे में उसका नाम लिया गया। उसे चुराने वाले मुर्गीचोर कह कर चिढ़ाये गए। रईसों के दस्तरख्वान की रौनक़ होते हुए भी ग़रीबों के शोरबे दाल के साथ तुल गई।
कहीं वो मुहावरे में नाम लेकर दिए गए सम्मान को लौटाने की तो नहीं सोच रही?

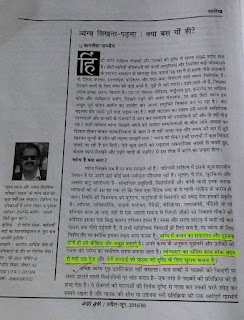

Comments