हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका "हरिगंधा" के व्यंग्य विशेषांक में प्रकाशित मेरी व्यंग्य रचना
गरीबों की सुनो
गरीबी एक जिद्दी सी चीज़ है जो हटाये नहीं हटती. यहाँ तक कि सरकारों की ‘गरीबी
हटाओ’ के हुंकारों से भी नहीं डरती. जहां होती है, वहीं जमी रहती है, बल्कि
थोड़ा-थोड़ा पिघल कर आस-पास रिसती भी रहती है. आजादी के वक़्त देश में बहुत-सी गरीबी
पड़ी थी, पर तब सरकार के पास ढेरों दूसरे काम पड़े थे. योजनायें बनाना उनमें प्रमुख
था. सरकार समझती थी कि योजनाओं की मदद से संपन्न होने वाले बड़े-बड़े कामों से जो
समृद्धि पैदा होती है उसकी तलछट से गरीबी भी हटती जाती है. जैसे एक बड़ा बाँध बनाने
से उसके डूब-क्षेत्र में रहने वाले गरीब हटा दिए जाते हैं तो गरीबी भी उनके साथ ही
हट जाती है. कुछ दशकों के बाद पता चला कि गरीबी हट तो गयी थी पर उन ग़रीबों के साथ
वहीं जाकर बस गयी जो अब भी गरीब ही हैं. तब विशेष तौर पर ‘गरीबी हटाओ’ का
हुंकार-भरा नारा दिया गया. तब से सरकारें गरीबी हटाने में जुटी हैं, बल्कि अब तो
गरीबी-उन्मूलन की बात करने लगी हैं.
गरीबी हटाने के सिलसिले में सरकार ग़रीबों की गिनती करवाने के अलावा गरीबी की
नाप-जोख भी करवाती है. सरकारी विद्वान गरीबी की परिभाषा तय कर एक लक्षमण-रेखा सी खींच
देते हैं. इस रेखा के नीचे वालों को ऊपर फेंकने की क्रिया को ही गरीबी हटाना कहते
हैं. जब सरकार का ये मानने का जी करता है कि गरीबी हट रही है तो इस परिभाषा में
ज़रा-सी तब्दीली कर देती है, जिससे रेखा के नीचे चिपके लोग भगदड़ की शकल में ऊपर चढ़
जाते है. गौर कीजिए तो मानुष तन को चाहिए क्या? दो रोटी, तन ढकने को एक कपड़ा और सर
पे छप्पर. अब थोड़ा और गौर कीजिए तो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ पहला यानी दो-रोटियाँ
ही अनिवार्य है. बिना कपड़ों के रहना तो अमीरों के फैशन में भी शामिल है और रही बात
रहने-सोने की तो इतनी सारी ज़मीन तो कायनात ने दी है और सरकार ने भी काफी सडके और
फुटपाथ बनवाये हैं, कहीं पसर जाओ. अगर छप्पर की ही जिद है तो सरकार योजनाओं से जो
पुल, फ्लाईओवर बनते हैं, उनकी छाया ग़रीबों के काम क्यों नहीं आ सकती. इसीलिए सरकार
ने तय किया कि गरीबी की रेखा ज़िंदगी की रेखा पर टिकी मानी जायेगी. जितने में दो
जून दो रोटियाँ मिल जाएँ उतना कमाने वाले रेखा के उस पार. इस स्थापना के बाद पहले
तो गरीबी के पाँव ज़मीन से उखड़ते मालूम हुए पर जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जड़ें बहुत
गहरे गड़ी हैं, परिभाषा की खुरपी से केवल सतह भर खुदती है.
खाकसार, जिसे आपका मन हो तो विद्वान भी कह सकते हैं, ये विचार रखता है कि
गरीबी कई रेखाओं का एक जाल है जिसमें उलझे लोग दायें बाएं, ऊपर नीचे या आड़े-तिरछे
चलते रहते हैं. ऊपर अमीरी और नीचे गरीबी
होती है. बीच में मिला-जुला या मिडिल क्लास होता है. गरीबी के स्तर वाले फंदे से
ऊपर चढ़ते हुए जैसे ही ये अहसास होता है कि अमीरी पास आ रही है, पता चलता है कि हम
तो अब भी वहीं लटके हैं, बल्कि कहीं दायें या बाएं ओर के फंदे में उलझे हैं. इसे
गरीबी की सापेक्षता का सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके अनुसार हर आदमी किसी और के
मुकाबले गरीब होता है. एक अमीर से दीखते आदमी के दिल से खुद से ज़्यादा अमीर को देख
जो सुलगती सी आह निकलती है वो एक गरीब की आह के मुकाबले ज़्यादा गर्म होती है. दिन
के पहले भोजन की प्याज रोटी निगलने के बाद निकले डकार में तृप्ति की मात्रा चार
कोर्स के वाईन-युक्त डिनर से उपजे डकार की तुलना में ज्यादा पाई गयी है. इस तथ्य
की रोशनी में सरकारी विद्वानों की ये मान्यता सही प्रतीत होती है कि 5-10 रुपये
में तैयार भोजन करने वाले प्राणी अमीर नहीं तो गरीब भी नहीं हैं.
गरीबी का बड़ा माहात्म्य है. इसके बिना अमीरी की कल्पना ही नहीं की जा सकती.
अगर पड़ोसी के पास चार गाड़ियां और कोठी में सिर्फ पांच नौकर हों तो आप अपनी छः
गाड़ियों और साढे पांच नौकरों के जत्थे को अपनी अमीरी का जलवा मान सकते हैं. ज़ाहिर
है उस हालत में वो पड़ोसी गरीब कहलायेगा. हालांकि इस तुलना की सीमा भी है. अंग्रेज़ी
में ‘ज़ेड’ के बाद कोई और अक्षर न होने के कारण इस श्रेणी की सुरक्षा पाये लोगों को
परस्पर तुलना का आधार न मिल पाने से उनमें काफी कुंठा देखी गयी है. सत्ताईस मंजिला
घर का प्रतिमान स्थापित हो जाने के बाद देश का हर कोठी-महल धारी गरीब ही कहलायेगा.
गरीबी एक बड़ी पवित्र अवस्था है. धर्म-ग्रंथों में भी गरीब बने रहने के गुणगान
हैं क्योंकि गरीब ईश्वर के निकट रहता है. जाने वो ईश्वर के निकट रहता है कि नहीं, पर
गरीबी की हालत में ईश्वर से जल्द भेंट होने की संभावना लगातार बनी रहती है.
द्वापर-युग में गरीबों को ये सुविधा मिली हुई थी कि वे ईशवर से बिना अपॉइंटमेंट
मिलने जा सकते थे और मिलकर वापस लौट भी सकते थे. तब शर्त इतनी भर थी कि अपने
दो-जून के राशन में से एक जून का भेट-स्वरूप ईश्वर को समर्पित करना होता था. ये
सुखद स्थिति है कि इन दिनों दिशा उलट कर वह परम्परा फिर चालू हो गई है. ईश्वर के
प्रतिनिधि अब गरीब की कुटिया में स्वयं पधारते हैं और श्रद्धा और डील-डौल के
अनुसार उसका एक या दो जून का राशन वहीं ग्रहण करते हैं. ये स्पष्ट नहीं कि ऐसा
प्रभु –गण जून महीने के बाकी दिनों और अन्य महीनों में भी करते हैं अथवा नहीं. सुदामा
जो है, कृत्य-कृत्य हो लेता है कि उसके घर का पवित्र होना पूरी दुनिया टीवी चैनलों
पर देख रही है. ईश्वर के साक्षात पधारने में अतिरिक्त कष्ट इतना ही है कि चावलों
को पकाने में ईंधन भी खर्च होता है जो ईंधन की कीमतों को देखते हुए गरीब को भारी
लग सकता है. घर में ही ईश्वर के दर्शन करने और चावलों का समर्पण कर देने के बाद
गरीब अब उस चमत्कार की आशा में भी नहीं रहता जो द्वापर के सुदामा को घर लौटने पर
दिखा था. आज का सुदामा ये भी जानता है कि घर या ईश्वर के दरबार में अगर उसने चावल
की पोटली खुद नहीं सौंपी तो भी किसी न किसी तरह उससे वसूल ली जायेगी.
एक ही अवसर है जब सुदामाओं की गठरी पर नज़र गडाए बैठे स्वघोषित प्रभुओं को गठरी
वसूलने के लिए हाथ जोड़ने से लेकर पाँव तक पड़ने पड़ते हैं. अपने वोट की गठरी बगल में
दबाये सुदामा इतराता है और झपट कर छीनने की कोशिश करो तो बिदक भी जाता है. वैसे
चुनाव के त्यौहार पर सुदामा बड़े काम आते हैं. प्रभु-गण अपनी शक्तियों, चमत्कारों
और आशवासनों के प्रदर्शन हेतु जो प्रवचन देते हैं उन्हें सुनने वालों की भीड़
इन्हीं सुदामाओं से बनती है. चुनाव-पर्व के तमाम उपादान भीड़, पोस्टर, विज्ञापन और
मेनिफेस्टो के केंद्र में गरीब ही रहता है. इसके संपन्न होते ही, उसकी इकलौती गठरी भी गायब हो जाती है और अगले पर्व तक
अपनी ठठरी को चलाये रखने में जुट, बल्कि जुत जाता है.
यही वजह है कि ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के पीछे का मूल भाव ‘गरीबी बचाओ’ है. हमारी
सहृदय सरकारें हमेशा गरीबी को लेकर संवेदनशील रही हैं. वे इस सत्य का संज्ञान लेती
हैं कि गरीबी की वजह से ही उनका अस्तित्व कायम है. गरीबी हटाने के कुछ स्थापित तरीके
हैं जिन्हें वो बस आजमाती रहती है. एक तो अपना विकास ही है. विकास के लिए उद्योग,
सड़क-पुल कुछ भी करो, शुरू में उसमें बहुत से गरीब लगते हैं. विकास हो जाने पर
ग़रीबों को हटा दिया जाता है. दौराने-विकास ग़रीबों को एक नायाब चीज मिलती है रोजगार
से हुई आमदनी, जिससे चलता है उसका खर्चा. ये तो हुआ विकास का मोटा अर्थशास्त्र,
आगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्रभावी हो जाता है. गरीब की आमदनी के प्रकाश में आते ही
मंहगाई उसको चरने आ जाती है. उधर मुनाफ़ा और घोटाला विकास को गरीबी से उलटी ओर मोड़
ले जाते हैं. दूसरा नायाब तरीका है –गारंटी. खाना, घर-बार, शिक्षा, रोजगार सबकी
गारंटी. इसे पाकर गरीब, गरीबी में भी आश्वस्त रहता है. रोजगार की गारंटी मिलते ही
वो काम करना बंद कर देता है,क्योंकि उसे न रोज़गार पूरा मिलता है न पैसा. सरकार को
गरीबी हटने के आंकड़े ज़ुरूर मिल जाते हैं.
एक कालजयी गीत है- गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा ..तुम एक पैसा दोगे, वो
दस लाख देगा. दस लाख देने वाला गरीब क्यों है -ये दस लाख का प्रश्न है. ज़ाहिर है
गरीब का एक वोट दस लाख का है और दस लाख वोट मिल जाएँ तो नेता की पीढियां तर जाती
हैं. बदले में एक पैसा किसी भी शक्ल में दे दो- सौ का नोट, एक बोतल या ढेरों तरतराते
आश्वासन. बाक़ी उसकी सुन भर लो, वोट मिल जाने पर अनसुनी ही होनी है. करने वाला तो
उसके मामले में वैसे भी ईश्वर ही है. गरीबी मिटाकर गरीब को क्यों मारते हो. वे
ख़त्म हो गये तो तुम्हारी कौन सुनेगा.

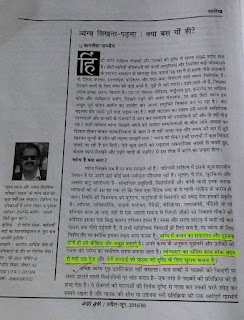

Comments