कबीरा घिरा बाज़ार से- vyangya
This is one of my favorite articles published in a family magazine "Vanita" last year. Enjoy...
कबीरा घिरा बाज़ार से
-कमलेश पाण्डेय
मैं निहायत कंजूस,
दकियानूस, पिछड़े खयालात का और इन ख़ूबियों की वज़्ह से एक जिद्दी, खड़ूस, नालायक और
निकम्मा आदमी हूं। हाल के कुछ सालों में मुझे ये आईना मेरी अपनी ही श्रीमतीजी
तक़रीबन रोज़ ही दिखाती रही हैं, हालांकि वो मेरी तारीफ़ में इनमें से एक दो लफ़्ज़ ही
कहती हैं, पर उनको बयान करने में वो अपनी ज़ुबान के अलावा चेहरे पर मौज़ूद बाकी
अंगों के साथ अपने हाथों का इतना प्रभावी इस्तेमाल करती हैं कि एक ही लफ़्ज़ में ऊपर
बताये गये तमाम और कुछ अनकहे और छूट गये विशेषणों का भी लुत्फ़ आ जाता है।
कंजूस तो मैं
अव्वल दर्ज़े का हूं। बक़ौल श्रीमतीजी, इसकी हद ये है कि महज़ तीन-तीन सौ के सिनेमा
टिकट खरीदने के डर से मैं उन्हें हर हफ़्ते सिनेमा नहीं ले जाता। अगर कभी ले भी गया
तो वहां केवल सौ-सौ रुपये में मिलने वाले पॉपकार्न और कॉफ़ी नहीं मंगाता। अगर मंगा भी
लूं तो मुंह बिचका कर खाता-पीता हूं। उनका खयाल है वो पनियल कॉफ़ी मुझे सिर्फ़
इसलिये कड़वी लगती है कि ये मुझे कहीं और के मुक़ाबले चार गुनी मंहगी मालूम होती है
। कंजूसी के कई और कीर्तिमान मेरे नाम हैं। हर हफ़्ते जाने योग्य एक और जगह है जहां
पार्किंग के पचास देने से बचने के लिये ही मैं जाने से कन्नी काटता हूं। ये जगह
है- शॉपिंग मॉल, जहां अगर चला भी गया तो वहां पाई जाने वाली दुकानों में घुसने से
गुरेज़ करता हूं। यहां भी सिर्फ़ उसी मामूली वज़्ह से कि यहां हर चीज़ की कीमतें दो से
ढाई गुना ज्यादा होती हैं। कंजूसी की बाबत श्रीमतीजी का एक सीधा आरोप मुझ पर ये भी
है कि घर में पका खाना मुझे दुनिया में सबसे लज़ीज खाना इसलिये मालूम होता है कि
मैं हफ़्ते में एक बार भी रेस्तोरां में जाकर अपनी ज़ेब हल्की करने से डरता हूं।
बल्कि उनका तो यहां तक मानना है कि लज़ीज खाना खुद ही बनाने का शौक़ मैंने जान-बूझ
कर इसीलिये पाला है कि घर में सबको बहका सकूं कि घर में ही जब इतना बढ़िया खाना
सस्ते में बन जाता है तो बाहर क्यों जायें।
आधुनिक जीवन शैली
के प्रति तो मेरा दृष्टिकोण बेहद संकुचित है- ये श्रीमतीजी द्वारा मेरे उपरोक्त
चारित्रिक पहलुओं के खुलासे के बाद साफ़ दिखा। मेरी सोच जो है वो एक प्रागैतिहासिक
घड़े की तरह है जो परंपराओं, नैतिकता और तार्किक चिंतन की पर्तों के नीचे दबी है।
ज़ुरूरी है कि इस सारे मलबे को खोद कर हटाया जाये और मेरी सोच को बाहर निकाल कर
आधुनिक तेज़ाबों से चमकाया जाये।
मेरी कई हरक़तों का
संबंध मेरी कंजूस मनोवृत्ति और बासी खिचड़ी सी मानसिकता के मिले-जुले असर से है। इस
वज़्ह से मैं पति होने का ये फ़र्ज़ कि वो पत्नी की ख़ूबसूरती की दिन-रात तारीफ़ करता
रहे, कुछ ज्यादा ही तत्परता से निभाता हूं। श्रीमतीजी साफ़ कहती हैं कि उन्हें
देख-देख कर मुग्ध होने का नाटक मैं अक्सर इसीलिये करता हूं कि इन दिनों
अनिवार्य-से हो चले ब्यूटी-पार्लर और फ़िटनेस सेंटर के ख़र्चे से बच जाऊं। वे तो ये
भी कहती हैं कि इधर जो चर्बी की पर्तें उनकी कमर और ज़िस्म के दीग़र हिस्सों पर चढ़
आईं हैं मुझे इसलिये नर्म और सुहानी लगती हैं कि उन्हें वो किसी सीसी नामक संस्था
से प्रति किलो पांच हज़ार की दर से पिघलवाना चाहती हैं। महिलाओं के इस आधुनिक
कर्मकांड से बिदकने का सिवाय इसके कोई कारण नहीं हो सकता कि मैं आधुनिक नारी-जीवन
में इनके महत्व से अनजान या पूर्वाग्रह से भरा हुआ हूं। एक रोज़ उनके लम्बे, काले, घुंघराले
रेश्मी बालों को अचानक अजीब सी रंगत लिये सपाट होकर कंधों तक सिमट आया देख मैंने
अपनी आपत्ति जताई तो उसके पीछे मूल वज़्ह ये थी कि उनके खयाल से बालों के इस
अनिवार्य रखरखाव और मेरे नज़रिये से अपने ख़ासे सुंदर बालों की छीछालेदर के लिये
उन्होंने ढाई हज़ार क़ीमत भी अदा की थी।
हद ये भी है कि
अपने पिछड़े दकियानूसी नजरिये को लेकर मैं ख़ासा अड़ियल हूं और पूरी बेशर्मी से उनका
बचाव करता और पोसता हूं। इसके उलट श्रीमतीजी जिस समाज में उठती बैठती हैं वह रोज़
आधुनिकता के नये-नये आयाम ढूंढता और अपनाता चलता है। एक दिन उनकी पूरी मंडली कटे
केशों और फंसे-फंसे ड्रेसों में ऊंची एड़ियों पर डगमगाती जाती दिखी। मालूम हुआ कि
यूं ही बैठे-बैठे बोर हो जाने की वज़्ह से ये लोग किसी मॉल में ‘आउटिंग’ के लिए निकल पड़ी हैं। मुझमें एक बड़ी कमी ये है कि कभी बोर नहीं होता, सो नये
दौर के बोरियत मिटाने वाले सामानों को आजमाने से रह जाता हूं। आधुनिक रवायतों से
बचने के एक से एक पैंतरे मैंने सीख रखे हैं।
श्रीमतीजी ने मेरी
दकियानूसी बुद्धि पर अंतिम मुहर लगाते हुए एक रोज़ मुझे ‘बुड्ढा’ करार दिया। बीते दिनों की स्मृतियों को साफ़ नकारते हुये उन्होंने अपना मंतव्य
यों दिया कि मैं तो जवानी की दलहीज़ पर पांव रखते ही सीधे पिछवाड़े की दिशा में चल
पड़ा और दस कदम में पूरी जवानी नाप कर बाहर निकल गया था। उनका सीधा मतलब था कि जो
काम नौजवान लोग करते हैं मसलन घूमना-फिरना, सिनेमा देखना वगैरह, वो सब जवानी में
भी नहीं किया। हनीमून जैसी एक यात्रा पर गया भी तो वहां उनसे ज्यादा वादियों को
तवज्जो दी। इसकी वज़्ह एक ही रही कि मुझे कोई शौक ही नहीं है। ये लिखना-पढ़ना, सोचना-विचारना शौक तो कतई नहीं
कहे जाने चाहिये। न तो मुझे ब्रांड्स की तमीज़ है न लेटेस्ट ट्रेंड्स की। शादी की
घड़ी अब तक लटकाये घूम रहा हूं कि वक़्त तो बताती है और मोबाईल को महज फ़ोन समझता
हूं। इंटर्नेट पर भी साहित्य-संगीत और उनसे जुड़े जीवों से ही नेटवर्किंग करता हूं
और मौक़ा पाते ही पुरानी फ़िल्में और गीत डाउनलोड करने लगता हूं। उन्होंने मेरे वाले
इंटर्नेट को भी पिछ्ड़ा घोषित किया हुआ है, हालांकि मैं जानता हूं कि इसमें
इंटर्नेट का कोई दोष नहीं। आधुनिक साइंस की इन महान खोजों का यों दुरुपयोग करने का
मुझे आख़िर क्या हक़ है-अर्थात कोई नहीं। टी वी के मामले में मेरी घिसीपिटी
विचारधारा में कंजूसी और घुल जाती है और मुझे किश्तों पर एक बड़ी और नई तकनीकों से
लैस टीवी घर ले आने से रोक देती है।
अंत में अपनी
नालायकी और निकम्मेपन पर भी थोड़ी रोश्नी फेंक दूं। इस घनघोर गतिशील जमाने में भी
आज तक मैं सिर्फ़ नौकरी ही करता चला जा रहा हूं। श्रीमतीजी मुझे इस जमाने के
अर्थशास्त्र से रु-ब-रू रखने की जी-तोड़ कोशिश करती हैं पर मेरे भेजे में शेयर
मार्केट या यहां-वहां बचत-कर्जे और निवेश का जाल फैलाने का कोई गुर नहीं घुस पाता।
विडंबना ये है कि पेशे से मैं अर्थशास्त्री हूं और सरकारी आर्थिक नीति बनाने में
योगदान करता हूं। श्रीमतीजी को पक्का यक़ीन है कि वह नीति मेरी वज़्ह से ही ‘फ़्लॉप” होती रही है। नौकरी करते हुए भी लोग
कितनी सफाई से अपनी बचत में इज़ाफा कर पूंजी में तब्दील करते दिन-रात लगे हुए हैं
और मैं हूं कि तन्ख़्वाह में कुछ फ़ीसदी हर साल जुड़ जाने और एक दो रचनाओं के
पारिश्रमिक को ही आमदनी की इंतिहा समझता हूं। श्रीमतीजी ने हज़ारों बार मुझे
क्रीम-पाउडर से लेकर हीरों तक के व्यापार करने की प्रेरणा दी और समझाया कि इसके
बिना आधुनिक तरीके से सुखी नहीं हुआ जा सकता। पर मैं अपने टुटपुंजिये सुखों के
कुचक्र में उलझकर रह गया हूं और कुछ ऊंचा और बड़ा सोचने से कतराता हूं। श्रीमतीजी
ज़ोर देकर कहती हैं कि मैं अगर अब भी नहीं चेता तो ईश्वर भी मेरा कुछ नहीं बना
सकते। वे हैरान रहती हैं कि कोई कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें
और उन्हें पाने के मौके उसके सामने बिखरे हों और उसका मन नहीं ललके।
मैं इन दिनों श्रीमतीजी
की सूक्ष्म दृष्टि का कायल चल रहा हूं जिसने मुझमें ये तमाम दुर्गुण ढूंढ निकाले।
मेरे दोस्तों ने तो ख़ामख़्वाह ही मुझे एक खुले विचारों वाला आदमी बता कर बरगलाये
रखा था। सदियों से बीबियां अपने पतियों को उनसे ज्यादा जानती रही हैं सो ये तय
करने का हक़ भी सिर्फ़ उन्हीं को है कि उनके पति क्या हैं।। ज़रूर कहीं मुझमें कुछ
बासी पड़ा हुआ है जिसकी बू सिर्फ़ मेरी श्रीमतीजी ही सूंघ पाती हैं। आज मैं उनकी ही
सौगंध खाकर स्वीकार करता हूं कि आज के बाज़ार युग में वही सारे संज्ञा-विशेषण हूं जिससे
वे मुझे पुकारती हैं।
फ़ोन- 09868380502

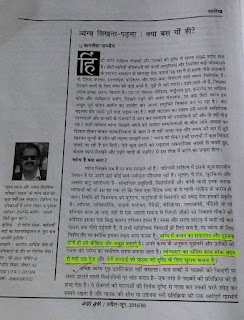

Comments
Regards,